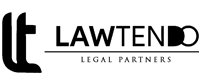दमन और दीव में सर्वश्रेष्ठ ट्रेडमार्क और कॉपीराइट वकील के साथ परामर्श करें
हम आपको दमन और दीव में सर्वश्रेष्ठ ट्रेडमार्क और कॉपीराइट वकीलों से परामर्श करने और नियुक्त करने में मदद करते हैं। अपनी खोज को कम करने के लिए फ़िल्टर का उपयोग करें और दमन और दीव में सर्वश्रेष्ठ वकील खोजें, चाहे आपका परिवार विवाद हो या तलाक का वकील, संपत्ति वकील, रोजगार या श्रम न्यायालय का वकील, आपराधिक वकील, वसूली या चेक बाउंस वकील, कराधान या कॉर्पोरेट वकील, या एक अनुभवी वकील किसी भी कानूनी विशेषता में
Get Legal Consultation
-
Advocate Babukumar Kannaiyan
विशेषज्ञता : सिविल कानून, तलाक और गुजारा भत्ता, मोटर दुर्घटना,...
शहर: कोयंबटूर
तजुर्बा : 13 वर्ष
प्रोफ़ाइल देखें -

-

Advocate J N Naresh Kumar
विशेषज्ञता : आपराधिक विधि, सिविल कानून, तलाक और गुजारा भत्ता,...
शहर: चेन्नई
तजुर्बा : 16 वर्ष
प्रोफ़ाइल देखें -

-

Advocate Srinivasa Rao Maddi
विशेषज्ञता : तलाक और गुजारा भत्ता...
शहर: विजयवाड़ा
तजुर्बा : 08 वर्ष
प्रोफ़ाइल देखें -

Advocate Prabal Parkash
विशेषज्ञता : आपराधिक विधि, तलाक और गुजारा भत्ता, मोटर दुर्घटना,...
शहर: करनाल
तजुर्बा : 03 वर्ष
प्रोफ़ाइल देखें -

Advocate Nikhil Rathod
विशेषज्ञता : आपराधिक विधि, सिविल कानून, तलाक और गुजारा भत्ता,...
शहर: पुणे
तजुर्बा : 01 वर्ष
प्रोफ़ाइल देखें -

Advocate Venkatesan Ramakrishnan
विशेषज्ञता : सिविल कानून, तलाक और गुजारा भत्ता, बीमा कानून,...
शहर: चेन्नई
तजुर्बा : 13 वर्ष
प्रोफ़ाइल देखें -

Advocate Swadha Kumari
विशेषज्ञता : आपराधिक विधि, सिविल कानून, बीमा कानून, पारिवारिक विवाद,...
शहर: लखनऊ
तजुर्बा : 08 वर्ष
प्रोफ़ाइल देखें -

Advocate Akshay Kumar
विशेषज्ञता : सिविल कानून, तलाक और गुजारा भत्ता, मकान मालिक...
शहर: उत्तरी दिल्ली
तजुर्बा : 04 वर्ष
प्रोफ़ाइल देखें -
दमन और दीव में सर्वश्रेष्ठ ट्रेडमार्क और कॉपीराइट वकील को खोजने के लिए मदद चाहिए ?
सहायता के लिए हमारे कानूनी विशेषज्ञों के साथ जुड़ें
विशेषज्ञ से बात करें
Lawyers for ट्रेडमार्क और कॉपीराइट in दमन और दीव
आमभाषा में 'कॉपीराइट' का अर्थ "संगीत, पुस्तक, नाटक, फिल्म, या किसी मूल रचनात्मक काम के उत्पादन और बिक्री को नियंत्रित करने का कानूनी अधिकार" होता है।
भारत में कॉपीराइट की सुरक्षा प्रदान करने वाला प्रमुख कानून प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (कॉपीराइट एक्ट, 1957) है।
इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, निम्नलिखित दो रूपों में कॉपीराइट सुरक्षा प्रदान किया जाता है: -
लेखक के आर्थिक अधिकार: कॉपीराइट में मूल साहित्यिक, नाटकीय, संगीत और कलात्मक कार्य शामिल हैं; सिनेमैटोग्राफी फिल्में, और साउंड रिकॉर्डिंग।
लेखक के नैतिक अधिकार: यह अधिनियम एक लेखक के निम्न नैतिक अधिकारों को परिभाषित करता है:
1. पितृत्व का अधिकार
2. अखंडता का अधिकार
न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए धारा 11 (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा कॉपीराइट बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष होता है (जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य होता है) और दो अन्य सदस्य (अधिकतम ११ सदस्य) होते हैं। अध्यक्ष के परामर्श के बाद, केंद्र सरकार कॉपीराइट के रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर सकती है, जो कॉपीराइट बोर्ड के सचिव होंगे और कुशलतापूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे।
भारत में कॉपीराइट कानून
धारा 12 (कॉपीराइट बोर्ड की शक्तियां और प्रक्रिया): धारा 12 (1) के अनुसार, बोर्ड के पास अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति है, जिसमें उसके बैठक के स्थान और समय को तय करना शामिल है।
बोर्ड अध्यक्ष द्वारा गठित बेंच के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यह प्रावधान ये स्पष्ट करता है कि कोई भी सदस्य किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेगा, जहाँ उसकी व्यक्तिगत रुचि है। इस बोर्ड द्वारा किए गए किसी भी कार्य या कार्यवाही को केवल बोर्ड के संविधान में किसी भी रिक्ति के अस्तित्व या दोष के आधार पर नकारा नहीं जा सकता है। इस प्रावधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कहता है कि कॉपीराइट बोर्ड को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 और 346 की दीवानी न्यायालय माना जाएगा, और बोर्ड के समक्ष सभी कार्यवाही को आईपीसी की धारा 193 और 228 के समानुपात में न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा।
धारा 13 (जिस कार्य में कॉपीराइट निर्वाह करता है): इस अनुभाग के अनुसार कॉपीराइट निम्नलिखित कार्यों में निर्वाह करता है:
मूल साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय और कलात्मक कार्य; सिनेमैटोग्राफ फिल्में; तथा ध्वनि रिकॉर्डिंग।
धारा 13 (a) मूल कार्यों की सुरक्षा करता है जबकि धारा 13 (b) और (c) उसके व्युत्पन्न कार्यों की रक्षा करता है।
धारा 14 (कॉपीराइट का अर्थ): धारा 14 के अनुसार किसी कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करना या उसके किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से को कॉपीराइट के नाम से जाना जाएगा, अर्थात्: -
क) साहित्यिक, नाटकीय या संगीत के काम के मामले में, कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं होना -
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किसी भी माध्यम में किसी भी भौतिक रूप या स्टोर में काम का उत्पादन करने के लिए
जनता को काम की प्रतियां जारी करने के लिए।
कार्य को सार्वजनिक करने के लिए, या उसे जनता तक पहुँचाने के लिए।
मूल निर्माता की अनुमति के बिना किसी भी सिनेमैटोग्राफ फिल्म या ध्वनि रिकॉर्डिंग बनाने के लिए।
कार्य को अनुकूल बनाने के लिए।
ख) कंप्यूटर प्रोग्राम के मामले में: -
बेचने या देने के लिए, या बिक्री या किराए के लिए प्रस्ताव, कंप्यूटर प्रोग्राम की कोई भी प्रति, चाहे इस तरह की प्रति बेची गई हो या पहले के अवसरों पर किराए पर दी गई हो।
कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 14 (a) की व्याख्या यह नहीं की जा सकती है कि अधिनियम की धारा 14 (e) (iii) के तहत जनता को अपने काम को बताने के लिए ध्वनि रिकॉर्डिंग के निर्माता का अधिकार खो गया है।
धारा 19 (समनुदेशन का तरीका/असाइनमेंट का तरीका): यह प्रावधान कॉपीराइट के कार्य के लिए शर्तों को पूरा करता है। यह एक आवश्यक शर्त है कि कॉपीराइट का समनुदेशन लिखित रूप में और हस्ताक्षरकर्ता या उसके विधिवत अधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, अन्यथा यह मान्य नहीं होगा। यह आवश्यक है कि कॉपीराइट के असाइनमेंट को ऐसे काम, अवधि और क्षेत्रीय सीमा को निर्दिष्ट करना होगा।
धारा 20 (कॉपीराइट का हस्तांतरण): इस खंड के अनुसार यदि कॉपीराइट के लेखक की मृत्यु हो जाती है, जो नाटकीय, साहित्यिक, कलात्मक, या संगीत कार्य की पांडुलिपि पर काम कर रहा था और मरने से पहले उसे प्रकाशित करने में सक्षम नहीं था, तो उस मामले में, उस कॉपीराइट का स्वामित्व उस व्यक्ति को प्रेषित किया जाता है जिसका नाम लेखक की इच्छा में बताया गया है।
ट्रेडमार्क क्या होता है?
ट्रेडमार्क IPR या बौद्धिक संपदा अधिकारों की एक शाखा है। बौद्धिक संपदा अधिकार लोगों को अपने अभिनव उत्पाद और रचनात्मक गतिविधि के स्वामित्व अधिकारों को बनाए रखने की अनुमति और सुनिश्चितता प्रदान करता है। बौद्धिक संपदा का विकास मानव श्रम के प्रयासों और कड़ी मेहनत के कारण ही हुआ है, इसलिए यह पंजीकरण के लिए कई आरोपों और उल्लंघन के आरोपों तक सीमित है। बौद्धिक संपदा के प्रकार ट्रेडमार्क, कॉपीराइट अधिनियम, पेटेंट अधिनियम और डिजाइन अधिनियम हैं।
एक उद्यम के ट्रेडमार्क में एक ऐसा नाम, शब्द या संकेत शामिल है जो अन्य उद्यमों के सामान या वस्तुओं से अपने सामानों या वस्तुओं को अलग करता है। ट्रेडमार्क का मालिक किसी अन्य प्रतियोगी द्वारा अपने चिह्न के उपयोग को रोक सकता है। ट्रेडमार्क व्यापार के वित्तपोषण को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण विपणन उपकरण है.
एक ट्रेडमार्क हमेशा एक ब्रांड नहीं होता है लेकिन ब्रांड हमेशा एक ट्रेडमार्क होता है। कभी-कभी ट्रेडमार्क और ब्रांड के बीच भ्रम होता है। ब्रांड नाम केवल एक प्रतीक या लोगो हो सकता है लेकिन ट्रेडमार्क एक व्यावसायिक संगठन में एक विशिष्ट संकेतक है क्योंकि इसमें ब्रांडों का व्यापक निहितार्थ है। लोग विशिष्ट ट्रेडमार्क से अधिक आकर्षित और प्रभावित होते हैं जो उत्पाद की गुणवत्ता को दर्शाता है। ट्रेडमार्क लोगो, चित्र चिह्न या नारा हो सकता है।
भारत में ट्रेडमार्क कानून: 1940 से पहले भारत में ट्रेडमार्क पर कोई कानून नहीं था। पंजीकृत और अपंजीकृत ट्रेडमार्क के उल्लंघन की कई समस्याएं उत्पन्न हुईं, जिन्हें विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 की धारा 54 के तहत हल किया गया था, और पंजीकरण भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत स्थगित कर दिया गया था। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, 1940 में भारतीय ट्रेडमार्क कानून लागू किया गया। ट्रेडमार्क कानून के लागू होने के बाद ट्रेडमार्क की सुरक्षा की मांग बढ़ी क्योंकि व्यापार और वाणिज्य में एक बड़ी वृद्धि दर्ज की गई।
ट्रेडमार्क कानून को ट्रेडमार्क और व्यापारिक माल अधिनियम, 1958 के साथ बदल दिया गया था। यह ट्रेडमार्क की बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है और माल पर दुरुपयोग या धोखाधड़ी के निशान के उपयोग को रोकता है। यह अधिनियम ट्रेडमार्क का पंजीकरण प्रदान करता है ताकि ट्रेडमार्क के मालिक को इसके विशेष उपयोग के लिए कानूनी अधिकार मिल सके।
इस पिछले अधिनियम को भारत सरकार द्वारा ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के साथ विश्व व्यापार संगठन द्वारा अनुशंसित TRIPS (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलुओं) के अनुपालन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। ट्रेडमार्क अधिनियम के पीछे मुख्य उद्देश्य ट्रेडमार्क के उपयोगकर्ताओं को पूर्ण सुरक्षा और संपत्ति की प्रत्यक्ष स्थिति के साथ-साथ कानूनी उपचार और ट्रेडमार्क अधिकारों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है।
ट्रेडमार्क का पंजीकरण: कोई भी व्यक्ति जो ट्रेडमार्क का मालिक होने का दावा करता है या भविष्य में उसके द्वारा ट्रेडमार्क का उपयोग करना चाहता है, वह एक निर्धारित तरीके से उपयुक्त रजिस्ट्रार को लिखित रूप में आवेदन कर सकता है। आवेदन में सामान, चिह्न और सेवाओं का नाम, वस्तुओं का वर्ग और ऐसी सेवाएँ शामिल होनी चाहिए जिनसे यह सम्बन्धित है। आवेदक का नाम और पता, और निशान के उपयोग की अवधि। यहां व्यक्ति का अर्थ फर्म, साझेदारी फर्म, एक कंपनी, ट्रस्ट, राज्य सरकार या केंद्र सरकार से है।
पंजीकरण की प्रक्रिया और अवधि: रजिस्ट्रार प्रोपराइटर द्वारा दिए गए आवेदन पर फीस के भुगतान के साथ, दिए गए अवधि के भीतर निर्धारित तरीके से ही ट्रेडमार्क जारी कर सकते हैं। एक ट्रेडमार्क का पंजीकरण दस साल का होगा और पंजीकृत ट्रेडमार्क का नवीनीकरण मूल पंजीकरण की समाप्ति की तारीख से दस साल के लिए या पंजीकरण के अंतिम नवीनीकरण के लिए भी होगा।
रजिस्ट्रार अंतिम पंजीकरण की समाप्ति से पहले नोटिस को पंजीकृत प्रोपराइटर को निर्धारित तरीके से भेजेगा। नोटिस में समाप्ति की तारीख और फीस के भुगतान का उल्लेख होता है, जिस पर पंजीकरण का एक नवीनीकरण प्राप्त किया जा सकता है यदि उस समय दिए गए समय की समाप्ति पर, उन शर्तों को रजिस्ट्रार के साथ विधिवत अनुपालन नहीं किया गया है, तो वे रजिस्टर से ट्रेडमार्क को हटा सकते हैं।
लेकिन रजिस्ट्रार ट्रेडमार्क को रजिस्टर से नहीं हटाएगा यदि निर्धारित प्रपत्र के भीतर निहितार्थ और निर्धारित दर ट्रेडमार्क के अंतिम पंजीकरण की समाप्ति से छह महीने के भीतर भुगतान किया जाता है और ट्रेडमार्क के पंजीकरण को दस साल के लिए नवीनीकृत करेगा।
यदि ट्रेडमार्क निर्धारित शुल्क का भुगतान न करने पर रजिस्टर से हटा दिया जाता है, तो रजिस्ट्रार छह महीने के बाद और ट्रेडमार्क के अंतिम पंजीकरण की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर पंजीकरण को नवीनीकृत करेगा, और निर्धारित प्रपत्र में निहितार्थ की प्राप्ति पर और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर रजिस्ट्रार ट्रेडमार्क को रजिस्टर में पुनर्स्थापित करता है और अंतिम पंजीकरण की समाप्ति से दस साल के लिए ट्रेडमार्क के पंजीकरण को नवीनीकृत करता है।
महत्वपूर्ण न्यायिक-फैसले :
हर्स्ट कंपनी बनाम दलाल एवेन्यू वर्बल एक्सचेंज लिमिटेड: इस वाद में अदालत ने कहा कि ट्रेडमार्क का उल्लंघन तब किया जाता है जब व्यापार के दौरान कोई और उद्यमी उस चिह्न का उपयोग करता है जो सामान के संदर्भ में ट्रेडमार्क के समान या भ्रामक है, जिसके संबंध में ट्रेडमार्क पंजीकृत है।
दक्षिण भारतीय संगीत कंपनियाँ बनाम भारत का संघ: इस मामले में, याचिकाकर्ता ने कॉपीराइट बोर्ड के कामकाज को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनी ढांचे को चुनौती दी। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि मौजूदा कानूनी ढांचा कॉपीराइट बोर्ड के सहायक के संरक्षण में विफल है। हालांकि, न्यायालय ने सहमति व्यक्त की कि बोर्ड में कम से कम एक न्यायिक सदस्य होना चाहिए।